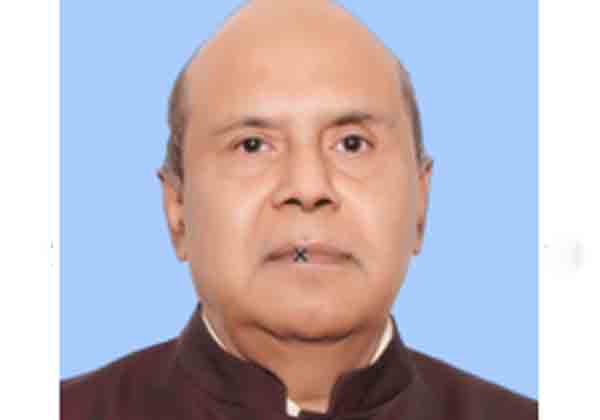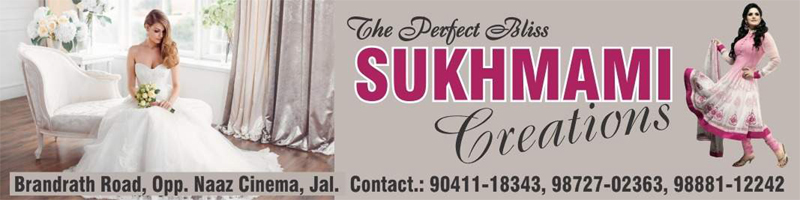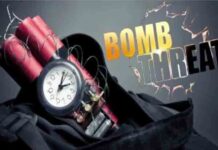Prabhat Times
कपूरथला। जब मैंने पहली बार महल को देखा, तो कपूरथला पर सर्दियों की हल्की- हल्की धूप पड़ रही थी। इसके गुंबद धुंध में हल्के से झिलमिला रहे थे, सैनिक स्कूल के मैदान के ऊपर किसी आधे-अधूरे सपने की तरह उभर रहे थे।
दूर से, यह असंभव सा लग रहा था मानो यूरोप से आई एक मृगतृष्णा पंजाब के मैदानों में उतर आई हो, जिसके गुंबद और बालकनियाँ एक लुप्त सदी की प्रतिध्वनि कर रही हों।
विशाल लोहे के द्वारों में प्रवेश करते हुए मैने स्वयं को एक आगंतुक कम और एक तीर्थयात्री सा ज़्यादा महसूस किया जोकि किसी दूसरे समय में प्रवेश कर रहा हो ।
प्रधानाचार्य, उप-प्रधानाचार्य और सैनिक स्कूल के एक शिक्षक ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया, उनके शिष्टाचार ने मुझे याद दिलाया कि चाहे इसका मूल वैभव बहुत पहले ही फीका पड़ चुका है परंतु यह अभी भी अनुशासन और कर्तव्य का स्थान है।
वे मुझे शांत गलियारों से होते हुए भित्तिचित्रों से सजी छतों, धूल से फीके पड़े झूमरों और पीढ़ियों के कदमों से चिकनी हो चुकी संगमरमर की सीढ़ियां दिखाते हुए ले गए। हवा में – कुछ तो उम्र की, कुछ तो उपेक्षा की – इतिहास की अपनी हल्की सुगंध थी ।
-
महाराजा और उनका सपना
एक सदी से भी ज़्यादा पहले, अह्लूवालिया राजवंश की राजधानी कपूरथला के महाराजा जगतजीत सिंह ने यहां अपना वर्साय बनाने का सपना देखा था।
1872 में जन्मे, ब्रिटिश संरक्षण में शिक्षित और पुनर्जागरणकालीन जिज्ञासा से समृद्ध, वे विरोधाभासों से भरे व्यक्ति थे – भीतर से भारतीय, फिर भी पूरी तरह से यूरोपीय रूचि रखने वाले।
ऐसे समय में जब उपमहाद्वीप अभी भी औपनिवेशिक शासन के अधीन था, जगतजीत सिंह ने पेरिस, लंदन और रोम की यात्रा की और कलाकारों, वास्तुकारों और राजनयिकों से समान सहजता से बातचीत की।
पेरिस ने उन्हें पूरी तरह से मोहित कर लिया था। उन्हें न केवल इसके मुख्य मार्गों और सैलून से, बल्कि यूरोप के मूल विचार से भी प्रेम हो गया – इसकी परिष्कृतता, कला और स्थायित्व के भ्रम से भी।
उनके लिए, फ्रांसीसी राजधानी विदेशी धरती नहीं, बल्कि उनकी अपनी आकांक्षाओं का दर्पण थी।
जब वह पंजाब में अपनी छोटी सी रियासत में लौटे, तो अपने साथ उस सपने का खाका लेकर आए – एक ऐसा महल जो यूरोप के सर्वश्रेष्ठ महलों को टक्कर दे सके, जो न केवल पत्थर से बना हो, बल्कि कल्पना से बना हो।
उन्होंने प्रसिद्ध फ्रांसीसी वास्तुकार एम. मार्सेल को इसका काम सौंपा और 1900 में काम शुरू हो गया।
दूर-दूर से सामग्री और कारीगर लाए गए-राजस्थान से संगमरमर, बेल्जियम से झूमर, वेनिस से दर्पण, ल्यों से टेपेस्ट्री।
इटली से लापीस लाजुली के स्तंभ और संगमरमर की चिमनियाँ आईं; फ्रांस से नाजुक प्लास्टर और फर्नीचर; और हॉलैंड से सैलून की सजावट के लिए चित्रकारी।
1908 में जब यह कार्य पूरा हुआ, तो जगतजीत पैलेस अपने सुंदर बगीचों के बीच चमचमाता हुआ खड़ा था, जो पूर्व और पश्चिम का एक दुर्लभ मिलन था।
वर्साय और फॉनटेनब्लियू की तर्ज पर बना यह महल पंजाब के समतल मैदानों पर लगभग लॉयर घाटी से आई मृगतृष्णा की तरह उभरा था।
इसके अग्रभाग 19वीं सदी की फ्रांस की ब्यू-आर्ट्स शैली में सजे थे, जिन पर लूवर की तरह अंडाकार खिड़कियों वाली मैनसार्ड छतें थीं।
स्वागत कक्ष का नाम सूर्य राजा लुई चौदहवें के नाम पर रखा गया था, जिनके शासनकाल ने फ्रांसीसी दरबार की भव्यता को परिभाषित किया था, जगतजीत सिंह जिसकी नकल ईंट, संगमरमर और प्रकाश में उतारना चाहते थे।
समकालीन लोग इसे पंजाब का पेरिस कहते थे। आगंतुकों को यह एक ऐसे व्यक्ति की कृति प्रतीत होती थी जो समय को थमा देने के लिए दृढ़ था – एक ऐसा महल जिसका बाहरी भाग फ्रेंच और आत्मा पंजाबी बोलती थी।
पंजाब का पेरिस
जगतजीत महल का अग्रभाग जीर्ण-शीर्ण अवस्था में भी मनमोहक बना हुआ है।
इसके नव-शास्त्रीय स्तंभ, मेहराबदार खिड़कियाँ और बांसुरीनुमा भित्तिस्तंभ सीन नदी के किनारों के साथ-साथ दोआबा के मैदानों से भी जुड़े हुए प्रतीत होते हैं।
लौवर और फॉनटेनब्लियू से प्रेरित गुंबददार मंडप, बेले एपोक की प्रतिध्वनि की तरह चमकता है।
जैसे ही मैं इसके स्तंभयुक्त बरामदे से गुज़रा, मुझे ऐसा लगा मानो महाराजा स्वयं दिखाई दे रहे हैं – रेशमी पगड़ी और सिला हुआ कोट पहने एक लंबा, सुंदर व्यक्ति, यूरोप और भारत से आए मेहमानों का स्वागत कर रहा था।
ऐसा कहा जाता था कि जब महाराजा भोज आयोजित करते थे, तो इन हॉलों में एक जीवंत ऑर्केस्ट्रा का संगीत गूंजता था, और महल के बगीचों से गुलाबों की खुशबू बालकनियों तक पहुँचती थी जहाँ मेहमान तारों के नीचे फ्रांसीसी शराब का आनंद लेते थे।
जगतजीत सिंह स्वयं अपने युग के राजकुमारों में एक विशिष्ट व्यक्ति थे। जैसा कि लाइफ पत्रिका ने उनके बारे में कहा था, वे “सबसे शालीन और महाद्वीपीय गुणों से युक्त” थे, एक ऐसे व्यक्ति जो हिमालय के पास अपने राज्य की तुलना में पेरिस के कैफ़े में ज़्यादा सहज महसूस करते थे।
वे साल का ज़्यादातर समय यूरोप में बिताते थे—मैक्सिम्स में भोजन करते, ओपेरा देखते, कलाकृतियाँ खरीदते—और हर सर्दियों में कपूरथला लौटते थे, उनके ट्रंक फ़र्नीचर, टेपेस्ट्री और इत्र से भरे होते थे।
दरबार की भाषा फ़्रांसीसी थी; उनके मंत्री उन्हें वोल्टेयर की भाषा में संबोधित करते थे; और उनका महल, मज़ाक में ही सही, शैटो कपूरथला के नाम से जाना जाने लगा था ।
वे चीनी मिट्टी के बर्तनों में भोजन करते थे, धाराप्रवाह फ़्रांसीसी बोलते थे, और यूरोपीय राजघरानों के साथ पत्र-व्यवहार करते थे। फिर भी, अपने तमाम पश्चिमी लिबास के बावजूद, जगतजीत सिंह कभी अपनी जड़ों से अलग नहीं हुए।
कपूरथला के महाराजा एक सिख राजकुमार थे जो यूरोप की नकल नहीं करना चाहते थे, बल्कि उसकी बराबरी करना चाहते थे—यह दिखाने के लिए कि भारत भी अपनी शर्तों पर सुंदरता का निर्माण कर सकता है।
महल के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। दरबार हॉल इसका दिल था—चमकदार वैभव से भरा एक स्थान, जो शीशों, तैलचित्रों और सोने के फ़र्नीचर से सजा था।
इसकी छत से एक इतना विशाल झूमर लटका हुआ था कि कहा जाता था कि उसे साफ़ करने के लिए एक दर्जन आदमियों की ज़रूरत पड़ती थी।
इतालवी कलाकारों द्वारा चित्रित इसके भित्तिचित्र, छनकर आने वाली रोशनी में चमक रहे थे। उनके नीचे, शीशम की लकड़ी से बने नक्काशीदार सिंहासन और सोफ़े अपने शाही निवासियों की प्रतीक्षा कर रहे थे।
हर कमरा एक कहानी कहता था। महाराजा के निजी अध्ययन कक्ष में चमड़े की जिल्द वाली किताबें रखी थीं—यूरोप के इतिहास, फ़्रांसीसी कविता के खंड, एटलस और कूटनीति पर ग्रंथ।
उनके संगीत कक्ष में पेरिस से मंगवाया गया एक भव्य पियानो था, जिस पर कभी मेहमान संगीतकार चोपिन और टैगोर जैसे संगीत बजाते थे।
एक दूसरे कक्ष में घड़ियों का एक संग्रह टंगा था, जिनमें से प्रत्येक एक यांत्रिकीय चमत्कार था, कुछ न केवल घंटे बल्कि चंद्रमा की कलाओं और तारों की गति का भी हिसाब रखती थीं।
महल दो सौ एकड़ में फैले सुंदर बगीचों, फव्वारों और मूर्तियों से सुसज्जित था। महाराजा के लिए, यह केवल एक शाही निवास नहीं था, बल्कि आधुनिकता का परिचय देता था—एक राजसी घोषणा कि भारत स्वाद और शिष्टता में यूरोप की बराबरी कर सकता है।
फिर भी, अपने सारे यूरोपीय लिबास के बावजूद भीतर से उनका जीवन पूरी तरह से भारतीय था जैसे- दरबार की लय, जनाना जहाँ महिलाएँ एकांत में रहती थीं, दरबार जहाँ प्रजा अपने शासक से प्रार्थना करती थी, और शाम के समय संगमरमर के गलियारों से आती चमेली की हल्की-सी खुशबू।
उनके पोते, ब्रिगेडियर सुखजीत सिंह के अनुसार, महल एक शांत स्मारक कम और एक निरंतर गतिशील स्थान ज़्यादा था—लिपिक, पहरेदार, नौकर और संगीतकार इसके कमरों में किसी भव्य बैले के पात्रों की तरह घूमते रहते थे।
शाम के समय, दरबार हॉल एक बॉलरूम में बदल जाता था, जहाँ महाराजा चमचमाते झूमरों और छत पर लगे रंग-बिरंगे तारों के नीचे नृत्य का शुभारंभ करते थे।
डिसूज़ा नामक एक गोवाई संचालक के नेतृत्व में दरबारी ऑर्केस्ट्रा वाल्ट्ज़ और फ़ॉक्सट्रॉट बजाता था, जबकि हीरे के आभूषणों वाले यूरोपीय मेहमान सफ़ेद टाई में लकड़ी के फ़र्श पर चक्कर लगाते थे।
ग्यारह बजते ही महाराजा चले जाते थे, और पीछे संगीत और सुगंध का एक भंवर छोड़ जाते थे—एक लुप्त दुनिया की गूँज।
दीवारों के भीतर की दुनिया
यूरोप के प्रति उनका आकर्षण उनके निजी जीवन तक भी फैला हुआ था। 1906 में, मैड्रिड में राजा अल्फोंसो XIII की शादी में शामिल होने के दौरान, जगतजीत सिंह को ग्रैन कुर्साल कैबरे में प्रस्तुति दे रही एक युवा स्पेनिश नर्तकी अनीता डेलगाडो से प्रेम हो गया।
उनकी मुलाक़ात एक किंवदंती बन गई—साम्राज्य और इच्छा से उपजी एक परीकथा। पत्रों और उपहारों के ज़रिए हुए एक संक्षिप्त प्रेम-प्रसंग के बाद, सोलह वर्षीय अनीता को पेरिस ले जाया गया, जहाँ उनके शिक्षकों ने उन्हें एक उपयुक्त जीवनसाथी में बदल दिया, और 1908 में वे कपूरथला की महारानी प्रेम कौर के रूप में भारत पहुँचीं—उनकी पाँचवीं और, अधिकांश विवरणों के अनुसार, उनकी पसंदीदा पत्नी।
उनके आगमन ने महल के जीवन को बदल दिया: वे अपने साथ फ़्लैमेंको की लय, सेविले की सुगंध और फ़िन-डे-सिएकल यूरोप की संवेदनशीलता लेकर आईं।
प्रेम कौर की कहानी भी उसी सुनहरे, ढ़लते हुए युग की है। पन्ने और फीते से लदी, वह महल में इस तरह घूम रही थी मानो उसकी संकर भव्यता का एक जीवंत प्रतीक हो—आधा यूरोप, आधा भारत।
उसका सबसे प्रसिद्ध रत्न, एक अर्धचंद्राकार पन्ना जो कभी उसके पति के हाथी के माथे पर सुशोभित था, उसका विशिष्ट आभूषण बन गया।
उसने बाद में लिखा कि “उसने मुझसे कहा कि अब चाँद मेरा है, और मुझे उसे पहनने की चुनौती दी।” उसने ऐसा ही किया—उसके बालों में एक सुनहरे धागे से लटका हुआ, मानो आकाश के किसी टुकड़े की तरह चमक रहा हो।
उस युग की तस्वीरों में शाही जोड़ा धूप से जगमगाते बगीचों में पोज़ देता हुआ दिखाई देता है जैसे वह रेशम और मोतियों में, वह शाही वर्दी में, और उसकी मूंछों पर परफेक्ट वैक्स लगा हुआ है।
उनकी कहानी ई.एम. फोर्स्टर के उपन्यासों से मिलती-जुलती लगती थी—दो दुनियाओं के बीच झूलता एक असंभावित रोमांस। फिर भी, इस वैभव के नीचे, अकेलेपन और सांस्कृतिक असंगति की धाराएँ थीं। महाराजा का यूरोप के प्रति आकर्षण जितना सुंदरता के बारे में था, उतना ही अपनेपन के बारे में भी था।
1920 के दशक तक, महाराजा की पेरिस के प्रति संवेदनशीलता लगभग मिथक बन गई थी। उन्होंने पेरिस में पैवेलियन रखा, केवल एवियन जल पिया, और अपने गहने कार्टियर से मँगवाए, जिसने कपूरथला के हेडड्रेस को उन्नीस पन्नों से जड़े एक मुकुट में बदल दिया।
महल के भीतर, दैनिक जीवन रंगमंच की तरह रचा-बसा था। महाराजा के दरबारी संगीतकार सुर में सितार और वायलिन बजाते थे; उनके रसोइये पंजाबी व्यंजन और फ्रांसीसी पेस्ट्री, दोनों तैयार करते थे; उनके मेहमान फ्रांसीसी राजाओं और सिख पूर्वजों, दोनों के चित्रों के नीचे बैठकर राजनीति पर बहस करते थे।
जगतजीत सिंह का महल सभ्यताओं के बीच एक सेतु बन गया था—20वीं सदी के शुरुआती भारत की वैश्विक कल्पना का एक जीवंत रूपक।
फिर भी, विलासिता की सतह के नीचे एक युग के अंत का शांत विषाद छिपा था। राजकुमारों, महलों और पर्दों की दुनिया लुप्त हो रही थी, और जल्द ही स्वतंत्रता, मितव्ययिता और वैभव के धीमे क्षय ने उसे अपने आगोश में ले लिया।
दुनिया के बदलते ज्वार के साथ कपूरथला का वैभव फीका पड़ने लगा। जब ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हुआ, तो उसकी छाया में रहने वाली छोटी रियासतें भी लुप्त हो गईं।
ग्रहण
स्वतंत्रता के बाद, कपूरथला का भारतीय संघ में विलय हो गया और महाराजा – अब वृद्ध हो चुके थे – स्मृतियों में खो गए। वह महल जो कभी उनके स्वप्न का प्रतीक था, एक अवशेष बन गया।
कुछ वर्षों तक, वह खामोश और बंद पड़ा रहा, उसके बगीचे घने हो गए, उसके फव्वारे सूख गए।
फिर, 1961 में, उसके परिसर में सैनिक स्कूल की स्थापना हुई – एक ऐसा महान संस्थान जो राष्ट्र सेवा के लिए लड़कों को प्रशिक्षित करता था जिसने अनिवार्य रूप से एक शाही निवास को एक परिसर में बदल दिया।
राजकुमारों की हँसी की जगह कैडेटों के आदेशों ने ले ली; वायलिन की धुनों की जगह सुबह के बिगुलों ने ले ली। एक तरह से, महल ने अनुशासन और सम्मान की अपनी परंपरा को जारी रखा – लेकिन इसकी भव्यता क्षीण होने लगी।
आज भी, सैनिक स्कूल की संरचना का अधिकांश भाग सुरक्षित है, लेकिन समय और उदासीनता ने अपना काम कर दिया है।
दीवारें उखड़ रही हैं, छतें टपक रही हैं, भित्तिचित्र धुंधले पड़ रहे हैं। कला के प्रतीक के रूप में निर्मित यह महल आज एक अनाथ कृति के रूप में जीवित है – गर्वित, घायल, प्रतीक्षारत।
मेरा दौरा
इसी जागरूकता के साथ मैं इसके शांत कमरों से गुज़रा। प्रधानाचार्या ग्रुप कैप्टन मधु सेंगर, उप-प्रधानाचार्य कमांडर संदीप सिंह विर्क और स्कूल के शिक्षक एवं पूर्व छात्र श्री मुनीश शर्मा ने मुझे विशाल हॉल में मार्गदर्शन किया, उनकी आवाज़ें सन्नाटे में धीमी गूँज रही थीं।
वे महाराजा और जो कुछ बचा है उसे संरक्षित करने में स्कूल की भूमिका के बारे में श्रद्धापूर्वक बात कर रहे थे। मैं उनके दिलों में जुनून और तत्परता और गौरवशाली विरासत को संरक्षित करने के लिए और अधिक करने की प्रबल इच्छा देख सकता था।
एक सैलून में, रंगीन शीशों से छनकर सूरज की रोशनी एक सौ साल पुराने पियानो पर पड़ रही थी। आवेग में, मैंने उसकी कुंजियाँ दबा दीं।
मुझे आश्चर्य हुआ कि भीतर से एक स्पष्ट, परिपूर्ण स्वर उठा – एक भूत की आवाज़ जो अभी भी अपने खोल में जीवित थी।
एक पल के लिए, मैं समय के साथ बहते संगीत को लगभग सुन सकता था – बहुत पहले की एक शाम की धुंधली याद जब महाराजा के मेहमान अब अंधेरे हो चुके झूमरों के नीचे वाल्ट्ज़ पर नाच रहे थे।
पास ही, मैंने पीतल और मीनाकारी के अद्भुत शिल्प कौशल से सजी एक घड़ी देखी, जिसके जटिल गियर अभी भी धीमी गति से चल रहे थे मानो मरने को तैयार न हों।
उसके चारों ओर उस ज़माने का फ़र्नीचर बिखरा पड़ा था—नक्काशीदार कुर्सियाँ, मखमली सोफ़े, महोगनी की मेज़ें, हर एक खोई हुई शान का गवाह। पेंटिंग और मूर्तियाँ एकदम अव्यवस्थित खड़ी थीं, जोकि मकड़ी के जाले से आधी ढकी हुई थी।
ये महज़ वस्तुएँ नहीं थीं; ये एक लुप्त चेतना के टुकड़े थे—एक राजकुमार की संवेदनशीलता जिसने पूर्व और पश्चिम, आस्था और आधुनिकता, कला और राजनीति को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की थी। और अब, वे धूल की परतों के नीचे भुला दिए गए थे।
मैंने सोचा, इतना प्राचीन, विरासत से सराबोर एक राष्ट्र, ऐसे खज़ानों को गुमनामी में कैसे खो जाने दे सकता है? हम अपनी कहानी को संजोए उन्हीं पत्थरों की अनदेखी करते हुए सांस्कृतिक गौरव का दावा कैसे कर सकते हैं?
विलाप
यह उपेक्षा हृदयविदारक है। महल का *दरबार हॉल*, जो कभी शाही सत्ता का केंद्र हुआ करता था, अब उदासी भरी जीर्णता में खड़ा है—उसकी सोने की परत चढ़ी छत उखड़ रही है, उसके भित्तिचित्र टूट चुके हैं।
समय के साथ फीके पड़ चुके झूमर, रोशनी की आहट की तरह लटके हुए हैं। संगमरमर के फर्श पर उम्र के दाग हैं, और दीवारें गौरव की फुसफुसाहट को भूत में बदल रही हैं।
फिर भी, इस जगह की आत्मा बनी हुई है। हवा में स्मृतियाँ गूंजती हैं—राजसी जुलूसों की, संगीत और हँसी की, गुलाब जल और इत्र से महकती शामों की।
पंजाब की कोमल रोशनी में, महल आज भी भव्य दिखता है, उपेक्षा से इसकी सुंदरता कम नहीं हुई है, मानो कोई बूढ़ा अभिजात गरीबी के आगे झुकने से इनकार कर रहा हो।
जब मैं मुख्य प्रांगण में खड़ा था, सर्दियों का सूरज गुंबदों के पीछे ढल रहा था, मुझे एक ऐसा दर्द महसूस हुआ जो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों था।
यह केवल एक खंडहर महल नहीं था; यह हमारी उदासीनता का दर्पण था, इस बात का प्रतिबिंब कि हम कितनी आसानी से भूल जाते हैं।
निश्चित रूप से, यह स्मारक इससे बेहतर का हक़दार है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जैसे पेशेवर निकायों को इसके संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए।
यहाँ जीर्णोद्धार कोई विलासिता नहीं है; यह इतिहास के प्रति एक कर्तव्य है। क्योंकि एक बार ये भित्तिचित्र चले गए, एक बार ये हॉल ढह गए, तो हम कला से भी ज़्यादा खो देंगे—हमने स्मृतियाँ भी खो दीं।
गौरव के भूत
शाम ढल गई, और जैसे ही मैंने अपने मेज़बानों से विदा ली, मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। ढलती रोशनी में महल मंद-मंद चमक रहा था, उसके गुंबद सूरज की आखिरी किरणों को सोख रहे थे। लॉन शांत थे, फव्वारे सूख गए थे, फिर भी छाया राजसी बनी हुई थी – उदासीनता के बावजूद एक सपना कायम था।
मैंने तब महाराजा जगतजीत सिंह के बारे में सोचा – एक महानगरीय राजकुमार, कवि, स्वप्नद्रष्टा – और कल्पना की कि वे इन्हीं गलियारों में चल रहे हैं, आशा से भविष्य की ओर देख रहे हैं। शायद, अगर वे इसे अभी देख पाते, तो वे दुखी होते।
या शायद वे मुस्कुराते, यह जानते हुए कि सपने, महलों की तरह, मरते नहीं; वे बस सोते हैं, पुनः खोज की प्रतीक्षा में।
जैसे ही मैं विशाल द्वारों से बाहर निकला, मुझे आश्चर्य और दुःख का मिश्रण महसूस हुआ। जगतजीत महल भारत की सबसे असाधारण कृतियों में से एक है – एक ऐसा महल जिसने दो दुनियाओं की भाषा बोलने का साहस किया, न केवल एक व्यक्ति का, बल्कि कल्पना के युग का एक स्मारक है।
यह आज भी खड़ा है, जर्जर होते हुए भी चमकता हुआ, एक चेतावनी और एक वादा दोनों की तरह।
अगर हम ध्यान दें, तो यह फिर से उठ खड़ा हो सकता है – इसके झूमर जगमगा उठेंगे, इसका संगीत फिर से शुरू हो जाएगा, इसका संगमरमर पहले की तरह चमक उठेगा।
और शायद तब, भविष्य की किसी शाम के सन्नाटे में, पुराना पियानो फिर से बज उठेगा – इसके सुर समय के साथ उस महाराजा के अटूट सपने को समेटे हुए हैं, जिसने कभी पंजाब के बीचों-बीच पेरिस का एक छोटा सा टुकड़ा बसाया था।
——————————————————-





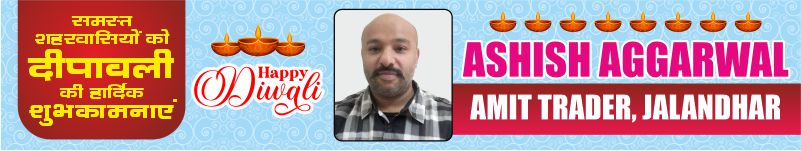
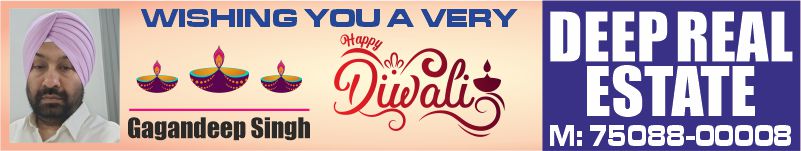



ये भी पढ़ें
- मान सरकार का शिक्षा में क्रांतिकारी योगदान : शिक्षकों के सम्मान और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए नया अध्याय शुरू
- ओ तेरी… DIG हरचरण भुल्लर के घर से मिला इतने करोड़ कैश, ज्यूलरी, जानें और क्या-क्या
- पंजाब सरकार का जनसेवा मॉडल ,₹510 CR की मेडिकल क्रांति ; होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर ने दी लाखों को नई जिंदगी
- वरिंदर सिंह घुम्मण के नाम पर रखा जाएगा डीसी और पुलिस कमिश्नर रेजिडेंस पार्क का नाम, नितिन कोहली 23 अक्तूबर को करेंगे उद्घाटन
——————————————————
 ————————————–
————————————–